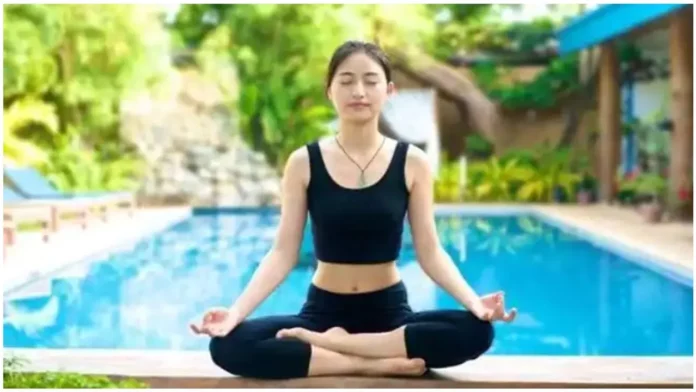कहते हैं योग को यदि पूरी तरह से और गंभीरता से अपना लिया जाए तो वह आदमी का सबसे अच्छा और भरोसेमंद मित्र साबित होता है। यह अपने साधकों को दु:खों और क्लेशों से मुक्त करता है और सुखपूर्वक समग्रता या पूर्णता में जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। वेदों से निकला हुआ ‘योग शब्द शाब्दिक रूप से ‘जुड़ने के अर्थ को व्यक्त करता है। अनुमानत: लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने ‘योग सूत्र में प्राचीन ज्ञान को कुछ सूत्रों यानी थोड़े से शब्दों से बनी संक्षिप्त शब्द-शृंखला में ग्रथित कर योग-विज्ञान के सिद्धांत और प्रयोग के निष्कर्षों को बड़े वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित कर लोक-कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य था मन में उठने वाली उथल-पुथल को रोकने, दैनिक जीवन में शांति स्थापित करने और अंतत: आत्मा और ब्रह्म का संयोग कराने के लिए मार्ग दिखाना। ध्यान, आसन, प्राणायाम और आध्यात्मिक नियमों के उपयोग को स्पष्ट करते हुए यह लघु ग्रंथ सहस्रों वर्षों से सबका मार्गदर्शक बना हुआ है। योग-दर्शन के अनुसार स्वास्थ्य और खुशहाली एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य की मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दशाओं के संतुलन और गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
वस्तुत: योग एक यात्रापथ भी है और यात्रा का लक्ष्य भी है। दिव्यता का निर्देश गुरु के माध्यम से मिलता है। यहां पर यह बताना भी उचित होगा कि दुर्गम जटिल संसार में दिव्य तत्व के प्रति समर्पण शांति पाने में लाभकर होता है। प्रभु-अनुग्रह के लिए समर्पण भी एक सक्रिय स्थिति या जीवन-प्रक्रिया है। परंतु योग के लिए यह समर्पण जरूरी नहीं है। निरीश्वरवादी भी योग में प्रवृत्त हो सकता है। स्मरण रहे कि शरीर-मन-संकुल में आने वाला सुधार केवल सतही उपकरण होता है। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है, क्योंकि यह न केवल शरीर-मन-संकुल का सुधार करता है बल्कि इसके समुचित उपयोग की विधि भी बतलाता है। योग का उपयोग हमें योग के अभ्यास का अवसर देता है। योग हममें से जो श्रेष्ठ है उसे उपलब्ध कराता है। चेतन रूप से योग का उपयोग जीवन को समृद्ध करता चलता है।
स्मरणीय है कि एक अध्ययन-विषय के रूप में योग भारतीय दर्शनों में से एक है। प्राय: सभी भारतीय दर्शन उस सर्वव्यापी परमात्म तत्व को स्वीकार करते हैं जो सभी विद्यमान वस्तुओं में उपस्थित है। व्यक्ति और उस परम सत्ता में एकात्मता होती है। योग मार्ग वह पाठ है जो व्यक्ति-चैतन्य को विकसित और समृद्ध करता है ताकि जीवन में अधिक सामंजस्य (हार्मनी) का अनुभव शामिल हो सके और अंतत: परमात्म तत्व के साथ एकता का अनुभव हो सके। जैसा कि उपनिषदों में वर्णित है हमारा अस्तित्व पांच कोशों से बनी रचना है। इस रचना में शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद के पांच क्रमिक स्तर पहचाने गए हैं।
योग का अभ्यास इन कोशों के बीच पारस्परिक संतुलन और चैतन्य लाता है और अस्तित्व के केंद्र परमात्म तत्व की ओर अग्रसर करता है। कह सकते हैं कि योग बाह्य से आंतरिक बुद्धि और आंतरिक से बाह्य बुद्धि की यात्रा है।
पातंजल योग-सूत्र बड़े ही सूक्ष्म ढंग से गूढ़ बातों को सामने रखते हैं। उन संक्षिप्त सूत्रों की विशद व्याख्या मनीषियों द्वारा कई तरह की जाती रही है। यह अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आठ अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सारे सूत्रों को चार अध्यायों या पादों: समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य, के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। इसी में पूरे योग-शास्त्र का विवेचन निबद्ध है। समाधि पाद में बताया गया है कि अहं के विचार के साथ अपना तादात्मीकरण और परमात्मा के साथ या उनके अंश के रूप में अपनी पहचान बनाना ही योग का मुख्य प्रतिपाद्य है। योगाभ्यास से चेतना का परिष्कार होता है ताकि मन परमात्मा की दिशा में अग्रसर हो। दु:ख और पीड़ा का अनुभव जो जो अहं के जुडऩे के फलस्वरूप होता है दूर हो और साधक प्रसन्नतापूर्वक जीवनयापन कर सके। एकाग्रता मुख्य प्रतिपाद्य है। साधन पाद का विषय क्रिया-योग है। मन में उठने वाले विघ्न को नियंत्रित करने की विधि बताई गई है। विभूति पाद में विभिन्न सिद्धियों या असाधारण शक्तियों का वर्णन किया गया है। चौथे, कैवल्य पाद में उस वास्तविक स्वतंत्रता की बात की गई है जो योग से मिलती है।
आत्म-ज्ञान के लिए अष्टांग योग के अभ्यास के अनुगमन, जिसे राज-योग भी कहते हैं, की संस्तुति की जाती है। योग के आठ अंग हैं न कि एक के बाद एक आने वाले चरण या सोपान। साधक को इन पर साथ-साथ समानांतर रूप से चलना चाहिए। योगाभ्यास का उद्देश्य साधक को आत्मावलोकन–अपने विचारों और व्यवहारों और उनके परिणामों को देखना-समझना भी होता है। यम और नियम नामक पहले दो चरण नैतिकता और सदाचारपूर्वक जीवन जीने के लिए निर्देश देते हैं। जहां यम बाहरी दुनिया के साथ सम्बन्ध पर केंद्रित हैं वहीं नियम निजी आध्यात्मिक विकास और आत्मानुशासन की आदतों को बताते हैं। यम पांच हैं : अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य (इंद्रियसुख का नियंत्रण) और अपरिग्रह (अनावश्यक वस्तुओं संचय/संग्रह)।
बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों के संयम को यम कहते हैं। पतंजलि ने इनको ‘महाव्रत कहा है जो जाति, देश और काल की सीमा से रहित सार्वभौम स्वरूप वाले हैं। यम वस्तुत: प्रतिबंध हैं जो सिर्फ कर्म के स्तर पर ही नहीं बल्कि विचार और शब्द के स्तर पर भी लागू होते हैं। इन यमों को अपनाने पर योगाभ्यासी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है और खुली सांस लेने का अवसर मिलता है। इनके अतिरिक्त पांच नियम हैं जो वस्तुत: सदाचार के पालन पर बल देते हैं। ये हैं: शौच (पवित्रता), संतोष, तप (इच्छाओं का शमन), स्वाध्याय (आध्यात्मिक ग्रंथों तथा स्वयं का अध्ययन) और ईश्वर-प्रणिधान (परमेश्वर को आत्मार्पण। इस तरह यम और नियम योग पथ के राही के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या करते हैं। ये आत्म शोधन का भी काम करते हैं और अच्छे तथा सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये नींव रखने का काम करते हैं।
आसन और प्राणायाम शारीरिक अभ्यास हैं पर इनका आध्यात्मिक महत्व भी है। आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख जीवन के लिए औजार भी ठीक होना चाहिए। राह मालूम हो लक्ष्य भी ज्ञात हो पर चालक ठीक है या नहीं यह भी देखना होता है। सोद्देश्य जीवन के लिए शरीर ठीक रखना जरूरी है। यह पवित्र कर्तव्य बनता है कि शरीर को स्वस्थ रखा जाए। प्राणायाम से प्राण ऊर्जा का संचरण शरीर में स्वेच्छा से होता है, सिद्धियाँ भी आती हैं और मन की स्थिरता भी। वस्तुत: प्राणायाम और प्रत्याहार दोनों ही आंतरिक दुनिया की ओर उन्मुख होते है और इस अर्थ में पहले के तीन चरणों- यम, नियम और आसान- से भिन्न होते हैं है। प्राणायाम का अभ्यास लयात्मक स्वास द्वारा इंद्रियों के अंदर की ओर खोजने की दिशा में चेतना को ले चलना, अंदर के अध्यात्म के गहन अनुभव की ओर अग्रसर करना संभव हो पाता है। पहले के पाँच चरणों द्वारा बाद के तीन चरणों के लिए उर्वर आधार भूमि का निर्माण करते हैं। धारणा योग का छठां चरण है। इसके अंतर्गत साधक अपने अवधान की एकाग्रता एक दिशा में और लम्बे समय तक बनाए रखता है। यह परमात्म तत्व पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी है। बिना किसी व्यवधान के निर्बाध ध्यान करना साधक को सहकार का अवसर देता है। साधक का समग्र अस्तित्व-शरीर, श्वांस, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ध्यान की वस्तु–सभी परमात्म तत्व के साथ एकीकृत हो जाते हैं। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव समाधि है जिसमें परमात्म तत्व के साथ एकाकार होना होता है। तब अलगाव का भ्रम दूर हो जाता है और आनंद के साथ परम चेतना के साथ एकत्व का अनुभव होता है।
आधुनिक युग में भारत में योग के ऊपर अध्ययन-अनुसंधान लगभग एक सदी से हो रहे हैं। पश्चिमी देशों में योग की लोकप्रियता बढऩे के साथ मनोचिकित्सा (थेरैपी) के रूप में इसके वैज्ञानिक विश्लेषण और शोध का तेज़ी से प्रचलन हुआ। अब अनेक मानसिक, सांवेगिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं जैसे दुश्चिंता (ऐंजाइटी), अवसाद (डिप्रेशन), पाचन क्रिया से जुड़े रोग, हृदय रोग, अस्थमा, मधुमेह और कैंसर आदि पर योग-अभ्यास के प्रभाव जाँचे समझे जा रहे हैं। चिकित्सा और मनोविज्ञान के अंतर्गत योग द्वारा आध्यात्मिक परिष्कार पर ध्यान नहीं दिया गया है जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण या जीवन के अनुभव को प्रभावित करता है। योगाभ्यास करने वाले प्राय: शरीर में विश्राम, मन में एकाग्रता और हृदय में शांति का अनुभव करते हैं। योग अपने को साधने की पराकाष्ठा या चरम बिंदु तक पहुंचा देता है। परंतु मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होता है। दिव्य या परमात्म तत्व ही उसे चरम उत्कर्ष (परफेक्शन) की ओर ले जाता है । परम तत्व से संयुक्त होना ही योग का लक्ष्य हो जाता है। वेदांत के दृष्टिकोण को मानें तो मनुष्य उसी दिव्य तत्व की प्रकट अभिव्यक्ति होता है। यह मिलन वस्तुत: आत्मान्वेषण हो जाता है। स्वयं अपने भीतर और सारे जगत में दिव्यता का दर्शन ही योग का अभीष्ट होता है।
-गिरीश्वर मिश्र