(मृणांक शेखर घोषाल- विनायक फीचर्स)
दुर्गोत्सव की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। पौराणिक काल से ही दुर्गापूजा होती चली आ रही है। ऋग्वेद में अंबिका, तैत्तिरीयारण्यक में उमा एवं हेमवती, नारायण उपनिषद् और दुर्गागायत्री में दुर्गा नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। देवी दुर्गा की पूजा का प्रसंग मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत, देवी पुराण और कालिका पुराण में भी मिलता है। मार्कंडेय पुराणानुसार मेधम ऋषि से दुर्गा का महात्म्य सुनकर चंद्रवंशी राजा सुरथ ने सर्वप्रथम उनकी आराधना की थी पर यह आराधना किस ऋतु में की गई थी, इसका उल्लेख नहीं मिलता। कहा जाता है कि उन्होंने वसंत ऋतु में देवीपूजा की थी।
कुछ विद्वानों ने इस कथा को ऐतिहासिक रूप देने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि वीरभूम जिले के बोलपुर के निकट स्थित सपुर के राजा सुरथ और बंगाल बिहार सीमा पर स्थित गौड़ देशवासी समाधि वैश्य ने अयोध्या के ब्राह्मण मेघस मुनि के निर्देशानुसार बंगला देश के चट्टग्राम के निकट स्थित करालडांगा पहाड़ के समीप बहने वाली कर्णफुली नदी के किनारे दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा की थी। वह पूजा शरद ऋतु में ही हुई थी। इसका प्रमाण चंडी ग्रंथ के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में मिलता है।
राम ने रावण के वध के लिए शरदकाल में देवी दुर्गा का बोधन किया था, जो अकाल में किये जाने के कारण अकाल बोधन कहलाता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के लिए दुर्गा की स्तुति की थी।
यूं तो दुर्गोत्सव का स्वरूप अब और भी निखर गया है और भारत के प्राय: सभी प्रांतों में किसी न किसी रूप में दुर्गा की आराधना की जाने लगी है, मगर अभी तक यह मतैक्य नहीं हो सका है कि दुर्गापूजा का ऐतिहासिक स्वरूप क्या है एवं ऐतिहासिक काल में दुर्गापूजा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। कुछ विद्वानों की अवधारणा है कि दुर्गापूजा को सार्वजनिक रूप सर्वप्रथम सेन वंश के राजाओं ने दिया था। गौड़ इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सेन वंश के राजा मैसूर राज्य से आकर गौड़वाना के सिंहासन पर आसीन हुए थे, फलत: उनकी संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का प्रभाव गौड़वानापर पडऩा स्वाभाविक था। दुर्गापूजा की अपनी विशिष्ट धारा को अक्षुण्ण रखने के लिए ही सेन राजाओं ने दुर्गापूजा का प्रचलन किया था। मैसूर के धारवाल जिले में ऐडोड़े नामक स्थान के निकट चालुक्य स्थापत्य के समृद्ध एक दुर्गा मंदिर विद्यमान है। कहा जाता है कि इसी दुर्गा मंदिर के अनुरूप बंगाल में प्रथम दुर्गा प्रतिमा निर्मित की गई थी।
एक ओर जहां यह विचारधारा प्रचलित है, वहीं दूसरी ओर यह कहा जाता है कि दुर्गापूजा का सार्वजनिक रूप 16वीं शताब्दी में स्पष्ट हुआ था। इसी समय शास्त्रोक्त और लौकिक दुर्गा में समन्वय स्थापित किया गया था। इस धारणा का पोषण करने वाले इतिहासकारों के अनुसार 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर के समकालीन एवं बांगला देश के राजशाही प्रांत के ताहिरपुर नामक क्षेत्र के जमींदार राजा कंसनारायण ने सर्वप्रथम दुर्गापूजा की थी और दुर्गोत्सव को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया था।
कहा जाता है कि राजा कंसनारायण यूं तो जमींदार थे मगर धर्म के प्रति उनकी प्रबल आस्था थी। एक बार उन्होंने अपने पुरोहित रमेश शास्त्री से महायज्ञ करने का आग्रह किया, मगर रमेश शास्त्री ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुए। कारण पूछने पर उन्होंने राजा से कहा: 'महायज्ञ चार प्रकार के होते हैं- (1) विश्वजीत, (2) राजसूय, (3) अश्वमेध और (4) गोमेध, विश्वजीत और राजसूय यज्ञ केवल वही राजा कर सकते हैं, जिन्होंने अन्य सभी राजाओं का राज्य जीत कर सार्वभौम राजा की उपाधि प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और सिर्फ एक भू-स्वामी राजा हैं। इसीलिए आपको विश्वजीत और राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है।'
राजा ने जब अश्वमेध यज्ञ के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की तो पुरोहित ने उत्तर दिया- 'दिग्विजयी राजा के अलावा और कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आपने चूंकि दिग्विजय नहीं किया है। अत: अश्वमेध यज्ञ आपके लिए वर्जित है। इसी तरह गोमेध यज्ञ भी इस युग में निषिद्ध है। ये चारों प्रकार के यज्ञ केवल क्षत्रिय राजा ही कर सकते हैं। आप राजा तो हैं, मगर क्षत्रिय न होकर ब्राह्मण हैं। फलत: इन यज्ञों में से एक भी यज्ञ करने का आपको अधिकार नहीं है।'
निराश और दुखी राजा के यह पूछने पर कि क्या करना उचित होगा पुरोहित ने कहा- 'आप दुर्गोत्सव का आयोजन कीजिए। राजा ने कभी दुर्गोत्सव का नाम नहीं सुना था। अत: वे दुर्गोत्सव के बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर बैठे। पुरोहित ने कहा- 'देवी दुर्गा की पूजा ही दुर्गोत्सव है। इस पूजा के करने से आपको सभी यज्ञों का फल प्राप्त होगा।'
राजा कंसनारायण ने तब रमेश शास्त्री को ही दुर्गापूजा का आयोजन करने के लिए कहा। राजा कंसनारायण की अध्यक्षता में पंडितों की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें राजपुरोहित रमेश शास्त्री ने दुर्गोत्सव मनाने के लिए सभा में उपस्थित सभी पंडितों का आवाहन किया और उनकी मदद मांगी। लंबे विचार-विमर्श के बाद रमेश शास्त्री ने पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की एक तालिका बनायी। उस तालिका में उलिल्खित सामग्री का संग्रह देश के विभिन्न स्थानों से किया गया। रमेश शास्त्री के ही निर्देशानुसार देवी दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण हुआ। मनुष्य के जीवन-यापन के लिए आवश्यक सभी तत्वों के प्रतीक उस प्रतिमा में सम्मिलित किये गये।
इस प्रकार राजा कंसनारायण के यहां दुर्गोत्सव प्रारंभ हुआ। कहते हैं, उस दुर्गोत्सव में साढ़े आठ लाख रुपए खर्च हुए थे। इस दुर्गापूजा के कारण सारे बंगाल में एक नयी चेतना फैल गई। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। राजा कंसनारायण का अनुकरण करते हुए अन्य लोग भी दुर्गापूजा करने लगे। फलत: दुर्गोत्सव ने धीरे-धीरे सार्वजनिक रूप ले लिया।
कुछ इतिहासकारों का मत है कि 19वीं शताब्दी में वंगाधिप हरिवर्मा देव के प्रधानमंत्री भवदेव भट्ट ने दुर्गापूजा की पद्धति की रचना की थी। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जीकन बालक और श्रीकर की पूजा पद्धति का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उनके पहले ही पूजा पद्धति लिखी जा चुकी थी। इसके अलावा यह पद्धति शारदीय महापूजा की है, वासंती पूजा की नहीं। वासंती दुर्गापूजा की पद्धति 'वासंती विवेक' की रचना शूलपाणि (1375-1460) ने की थी।
रमेश शास्त्री ने सिर्फ सपरिवार दुर्गापूजा का प्रचलन किया था। चाहे जो भी सही हो मगर यह तय है कि राजा कंसनारायण की दुर्गापूजा इतनी प्रभावशाली थी कि उससे प्रभावित होकर बादशाह शाहजहां हर साल अपने व्यय से बंगाल में दुर्गोत्सव का आयोजन करवाते थे। औरंगजेब के काल में यह परंपरा टूट गई।
राजा कंसनारायण की तरह भादुड़ा के राजा जगतनारायण ने भी दुर्गोत्सव का आयोजन करना चाहा था फलत: पुरोहित की सलाह पर बसंतकाल में बासंती दुर्गोत्सव का आयोजन किया गया।
राजा कंसनारायण की अपेक्षा ज्यादा धन खर्च करके जगतनारायण अधिकाधिक यश प्राप्त करना चाहते थे पर उनका प्रयास असफल रहा। कारण पूछने पर उनके पुरोहितों ने कहा- राजा कंसनारायण द्वारा भक्तिभाव से की गई पूजा का अनुकरण आपने ईर्ष्या के कारण किया था। उसमें भक्ति का अभाव था। इसीलिए आपकी पूजा सार्थक नहीं हुई।
यूं तो राजा कंसनारायण की दुर्गापूजा को ही सर्वप्रथम दुर्गापूजा की आख्या दी गई है पर यह कहां तक सच है, कहना बहुत मुश्किल है।





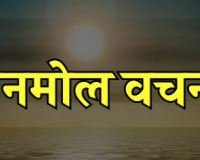
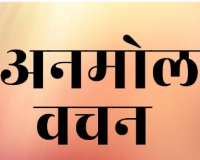







.jpg)


